प्रेमकुमार मणि, पटना:
रामस्वरूप वर्मा (22 अगस्त 1923 -19अगस्त 1998 ) का नाम नयी पीढ़ी के लिए अनजाना हो सकता है, क्योंकि उनकी वैचारिक-राजनीतिक धारा आज बिखर चुकी है. पिछले दशकों में कोटा -पॉलिटिक्स ने सामाजिक न्याय की राजनीतिक विचारधारा का गला घोंट दिया है. सब कुछ आरक्षण में समाहित हो गया है. स्थिति यह है कि जातिजनगणना भी आज सामाजिक परिवर्तनकारियों का कार्यक्रम बन जाता है. यह सब कोटा-पॉलिटिक्स के अपरूप हैं, जिसने धुंध अधिक फैलाई है. हम रामस्वरूप वर्मा की बात कर रहे थे. वह उनलोगों में थे, जिन्होंने सत्ता की नहीं, विचारों की राजनीति की. उत्तरप्रदेश विधानसभा के वह लम्बे समय तक सदस्य रहे और चरण सिंह के मुख्यमंत्रित्व में जब सरकार बनी, वहां वित्तमंत्री भी रहे. उनके द्वारा स्थापित सामाजिक -सांस्कृतिक संस्था "अर्जक संघ" ने किसान -दस्तकार जातियों के बीच वैज्ञानिक -मानवतावादी नजरिया विकसित करने का प्रयास किया. अर्जक का अर्थ है अर्जन करने वाला. मिहनतक़श तबका. किसान-कामगार-दस्तकार तबका. यह काऊ- बेल्ट अथवा गोबरपट्टी में हिंदुस्तानी मिहनतक़श जन के सांस्कृतिक जागरण का संगठित मंच भी था, जिसकी जरूरत आज़ादी के इर्द-गिर्द मानवेंद्रनाथ राय सरीखे लोगों ने महसूस की थी. बिहार के मशहूर नेता जगदेव प्रसाद ने उनसे ही प्रभावित होकर 1970 के दशक में अपनी पिछडावादी कोटा -वादी राजनीति को द्विजवाद विरोधी राजनीति में तब्दील कर दिया था.

हिंदी क्षेत्र में साठ के दशक में समाजवादियों के बीच जाति और वर्ण के सवाल गहराने लगे थे. यह शायद इस कारण हुआ था कि 1952 के आखिर में सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने दक्षिणपंथी गांधीवादी आचार्य कृपलानी के किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ विलय कर के प्रजा सोशलिस्ट बना ली और कृपलानी की जिद पर वर्ग संघर्ष की राजनीति को अलविदा कर दिया. कुछ समय बाद राममनोहर लोहिया ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए वर्ग की जगह चुपके से वर्ण को रख दिया और अपनी तरह के एक अहिंसक वर्ण -संघर्ष की प्रस्तावना कर दी. 1964 -65 में लोहिया के नेतृत्व वाली नवगठित संयुक्त समाजवादी पार्टी अर्थात संसोपा के नारे 'संसोपा ने बाँधी गांठ , पिछड़ा पावें सौ में साठ ' ने बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इससे जोड़ा था. इससे धारासभाओं में तो समाजवादी सदस्यों की संख्या बढ़ी किन्तु बड़े पैमाने पर जातिवादी तत्व भी पार्टी में भर गए. जातिवादी व्याधि ने सोशलिस्ट राजनीति को कुल मिला कर वैचारिक स्तर पर सुस्त बना दिया. देश- दुनिया की घटनाओं पर नजर और इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या करने में समाजवादियों का कोई जोड़ नहीं था. अब सब कुछ जाति -केंद्रित हो गया.

दक्षिण भारत में इसी समय पेरियार का आंदोलन चल रहा था और महाराष्ट्र में आम्बेडकरवादी भी राजनीति के ब्राह्मणवादी व्याकरण पर चोट कर रहे थे. लेकिन हिंदी पट्टी में ऐसा कोई सिलसिला नहीं चल रहा था. रामस्वरूप वर्मा जैसे लोगों ने अनुभव किया कि संसोपा इसे लेकर गंभीर नहीं है. बहस इस बात की भी थी कि आरक्षण और अवसर नहीं, इस वर्णवादी-जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने की जरुरत है. स्वयं लोहिया की गाँधी में आस्था थी. गाँधी की रामराज -वादी मानसिकता वर्णवाद को स्वीकृति देते थे. इसी सवाल पर आंबेडकर गाँधी से दूर हुए थे. रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद जैसे नेताओं ने गाँधीवादी लोहियावाद से मौन -विद्रोह किया और चुपचाप फुले-अम्बेडकरवाद के नजदीक आये. जीवन के आखिरी समय में कर्पूरी ठाकुर का भी गांधीवादी लोहियावाद से मोहभंग हो गया था. वह भी फुले-आम्बेडकरवाद से जुड़ाव महसूस कर रहे थे. आनेवाली पीढ़ियां जब जागरूक होंगी, इस राजनीतिक विकास का सम्यक अध्ययन प्रस्तुत करेंगी.

(प्रेमकुमार मणि हिंदी के चर्चित कथाकार व चिंतक हैं. दिनमान से पत्रकारिता की शुरुआत. अबतक पांच कहानी संकलन, एक उपन्यास और पांच निबंध संकलन प्रकाशित. उनके निबंधों ने हिंदी में अनेक नए विमर्शों को जन्म दिया है तथा पहले जारी कई विमर्शों को नए आयाम दिए हैं. बिहार विधान परिषद् के सदस्य भी रहे.)
नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं. The News Post का सहमत होना जरूरी नहीं. हम असहमति के साहस और सहमति के विवेक का भी सम्मान करते हैं.






.jpeg)

.jpeg)










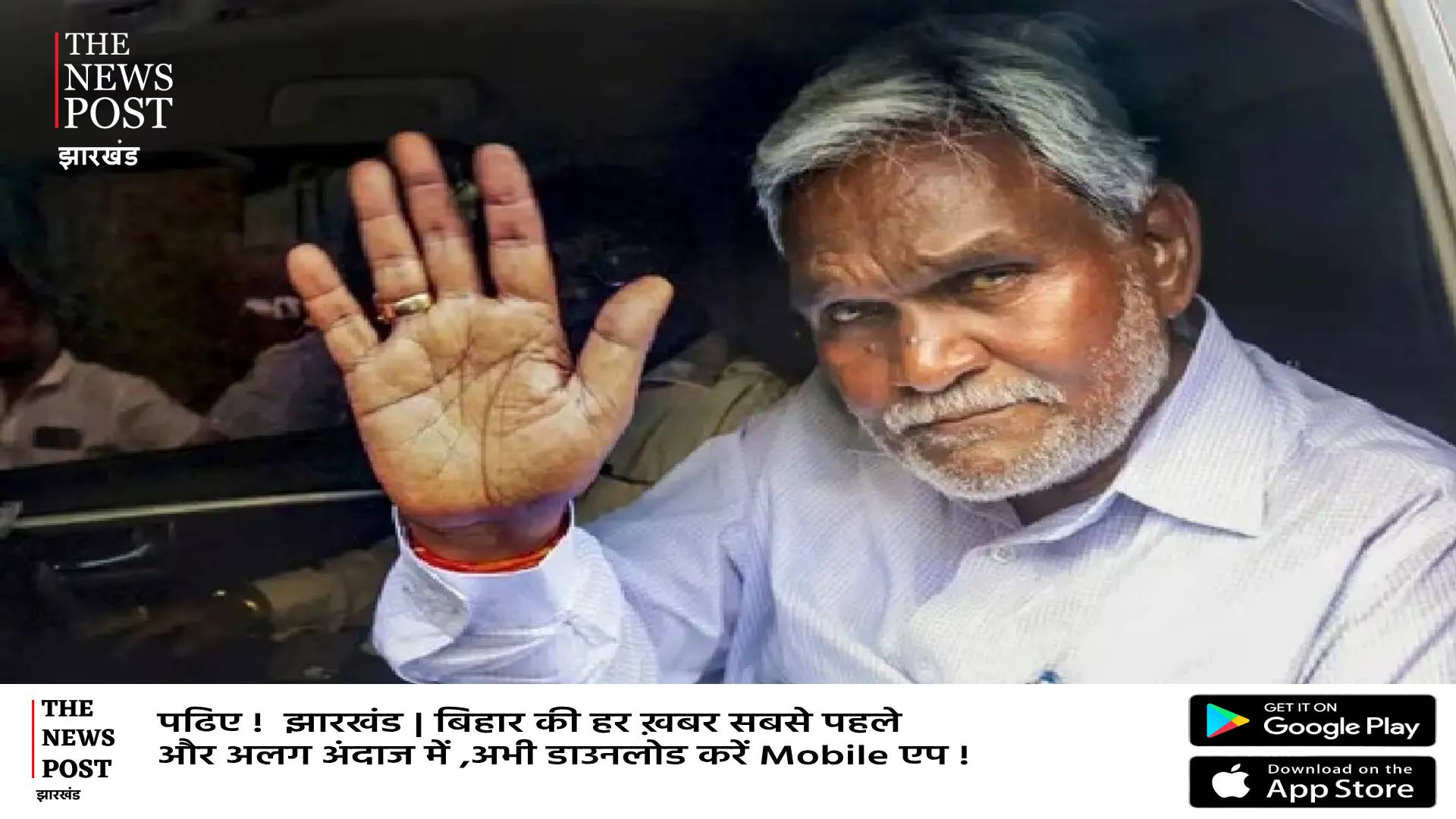
Recent Comments