टीएनपी डेस्क (TNP DESK): जिंदगी के अंतिम दिनों डॉ. रामदयाल मुंडा (23 अगस्त 1939-30 सितंबर 2011) बेहद अशक्त हो गए थे. आंखों की रौशनी धुंधली थी, पर कला-संस्कृति और साहित्य की योजनाओं पर दृष्टि उतना ही तेज़. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की समृद्ध संस्कृति को पहुंचाने वाले डॉ. मुंडा के बुज़ुर्ग हाथ आखिरी समय में भले कांप रहे थे, लेकिन कला को संरक्षित करने के लिए कागजों पर उनकी उंगलियां उतना ही तीव्र वेग से चलती रहीं. चाहते थे कि झारखंड के गीतों के संग्रह का एक संकलन प्रकाशित हो. उन्होंने स्वरचित गीतों-वाद्य यंत्रों के जरिये झारखंड को विश्व में पहुंचाने का अदभुत काम किया. डॉ मुंडा. ने एक ऐसे गीत की रचना की थी, जिसमें झारखंड की हर भाषा के शरद थे. उनकी चाहत थी कि 'हर बोल गीत और हर चाल नृत्य फिर जीवित हो उठे. उनको गुजरे 11 साल हो गए. इस दरम्यान उनके प्रिय संगी साथी बीपी केशरी, गिरिधारी राम गौंझू भी अपने पुरखा लोक में चले गए.
नृत्य-संगीत रामदयाल का मुंडा का एक अहम पक्ष
नृत्य-संगीत उनका एक अहम पक्ष है. उन्हें साहित्य नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला था और उनके संपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री भी. पर, इतने बड़े शहर में उनके काम, उनके अवदान, उनके सांस्कृतिक पक्ष, उनकी किताबों, विचारों, जीवन शैली आदि पर भी तो बात होनी चाहिए. जब हम बकौल मेघनाथ के शब्दों में-झारखंड का टैगोर कहते हैं, तो उस दिशा में भी पहल होनी चाहिए. टैगोर हिल के आसपपास लोगों ने कब्जा कर लिया और नगर निगम गरीबों के आशियाने उजाड़ता रहा. एक धरोहर के चारों तरफ कब्जे के कारण भारतीय पुरातत्व ने टैगोर हिल को अपने अधीन नहीं लिया. राजधानी का यह हाल है, जहां पूरे राज्य का तंत्र बैठता है.

खंडहर हो रहा उनका बनवाया भवन
टैगोर हिल के पीछे डॉ मुंडा ने एक भवन बनवाया था, आज खंडहर हो रहा है. दीवारों पर जगह-जगह दरारें पड़ चुकी हैं. खिड़कियां उखड़ च़की हैं. एक अकेले प्रभाकर नाग उनके उस सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, अपनी मृत्यु के एक सप्ताह पहले डॉ. मुंडा ने इसका शिलान्यास किया था. तब वे राज्यसभा के सांसद थे और सांसद कोटे से इसके लिए एक करोड़ की राशि दी थी. वे चाहते थे कि यहां एक ऐसा केंद्र बने, जहां सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो सके. एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकें. लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं. डॉ मुंडा. सिर्फ देश-विदेश के आदिवासियों के बीच ही पुल नहीं थे. भारतीय शास्त्रों के वे गहन अध्येता थे और शास्त्रों को देखने का उनका नजरिया भी था. उनकी हिंदी में एकमात्र छपी किताब में देख सकते हैं. दूसरी जो किताब है, वह है आदि धरम. वे सरना की बजाय आदि धरम को ही रखना चाहते थे. झारखंड आंदोलन को भी उन्होंने बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया. मोटरसाइकिल पर गांव-गांव घूमे. यह कम महत्वपूर्ण काम नहीं था. फिल्मकार मेघनाथ ने उनपर डाक्यूमेंट्री बनाकर अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया. इसे सबको देखना चाहिए.

हमें सिर्फ उनकी प्रतिमाएं ही नहीं गढऩी चाहिए, उनके सपनों को साकार करने की दिशा में भी काम करना चाहिए और उनके अकादमिक पक्ष पर भी बेहतर काम होना चाहिए. डा. रामदयाल मुंडा अमेरिका में रहे. वहां से पढ़ाई की. इसके बाद एक बुलावे में अपने 'देस’ लौट आए. अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपरा को सहेजने, आगे बढ़ाने, गति देने. वे शॉल वृक्ष की तरह थे. सभी आदिवासी उस विशाल वृक्ष की छाया में खुद को सुरक्षित पाते. चाहे झारखंड के आदिवासी हों, छत्तीसगढ़ के या सुदूर असम से लेकर उत्तर पूर्व के. जब भी कोई समस्या केंद्र सरकार और आदिवासियों के बीच पैदा होती, वे सदैव एक आवाज बनकर उभरे.

गांव-गांव अखड़ा था उनका सपना
जनसरोकार से जुड़े पत्रकार संजय कृष्ण बताते हैं कि डा. रामदयाल मुंडा की सबसे बड़ी खासियत थी माटी से लगाव. आधे हाथ का खादी का कुरता और पैंट, घुघराले बाल और आंखों पर चश्मा उनके व्यक्तित्व को गढ़ते थे. वे सादगी से भरे थे. उनके भीतर हमेशा बांसुरी का एक समधुर सुर अनवरत बजरी रहती थी. मांदर की थाप पर पांव थिरकते रहते थे. संगीत-नृत्य-साहित्य-भाषा की चौहद्दी उनके मन-मानस को व्यापक बनाते थे. अंतरराष्ट्रीय भाषाविद् के दिल में एक कवि भी बसता था. 'आदिवासी’ के पुराने अंकों में छपी मुंडारी की उनकी कविताएं उनकी संवेदना की जाहिर करती हैं. अपनी मातृभाषा मुंडारी के अलावा नागपुरी, पंचपरगनिया, हिंदी, अंगरेजी में गीत-कविताओं के अलावा गद्य साहित्य भी रचा है. वे आदिवासियों की एकजुटता को लेकर भी सदैव प्रयासरत रहे. वे अखड़ा के प्रबल हिमायती थे. गांव-गांव अखड़ा बनाना चाहते थे. उसकी पूरी रूपरेखा भी वे बनाकर गए हैं. ये सपने कैसे जमीन पर उतरे, यह जिम्मेदारी सरकार की भी है और उनकी भी, जिनके दिलों में डॉ मुंडा आज भी जीवित हैं.









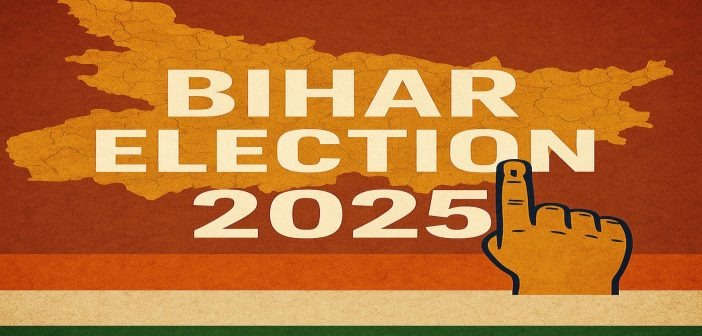








Recent Comments