TNP DESK ऋषि बंकिमचन्द्र का कहना था – “जिस राष्ट्र का अपना इतिहास न हो, उसके कष्टों का कभी अन्त नहीं हो सकता.” सुप्रसिद्ध इतिहासकार राधाकमल मुखर्जी के कथन में बंकिमचन्द्र पर की गयी उनकी टिप्पणी यहाँ दृष्टव्य है — “बंकिम ने इतिहास के अध्ययन के लिए निष्ठापूर्वक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई और सही अर्थों में ऐतिहासिक अनुसंधान की आधारशिला रखी.”
उन्होंने अपनी रचनाओं से जनमानस को झकझोर कर चेतन किया और नयी दिशा प्रदान की. बंकिम की कृतियों ने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच सेतु की भूमिका निभाई. उन्हें अगर पुनर्जागरण का सिपाही कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी.
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने 1838 ई. से 1894 ई. तक अपनी आरम्भिक रचना अंग्रेज़ी में लिखी. बाद में उन्होंने बंगला भाषा में लिखना प्रारम्भ किया.यह भी एक तथ्य है कि बंकिमचन्द्र ने बंगला भाषा को मात्र सुधार कर सामान्य उपयोगी ही नहीं बनाया, वरन् बंगला भाषा के साहित्य में एक युगान्तरकारी प्रभाव डाला और चमत्कार पैदा किया. बंगला साहित्य के आधुनिक काल को ‘बंकिम युग’ के नाम से जाना जाता है.
बंकिमचन्द्र का प्रथम उपन्यास है ‘दुर्गेशनंदिनी’. उनका औद्देश्य, देश-जाति के प्रति उनकी आस्था, आकांक्षा, उनको ऐतिहासिक इतिहास पर दृढ़ विश्वास— इन्हीं कारणों से उनके उपन्यासों में कहीं महाकाव्य की विशालता और कहीं गीतिकाव्य की अनुभूति आ जाती है. इतिहास को सत्य रूप में ग्रहण किया है, इसका आभास नहीं मिलता.
‘आनन्दमठ’ में सन्यासी-विद्रोह को उन्होंने ऐतिहासिक रूप में चित्रित किया है.
वस्तुतः देशप्रेम की भावना को व्यंजित करने के लिए यथार्थवादी साहित्यकार की अपेक्षा उससे ऊँचा लेकर बंकिम की मनीषा को जागृत करना पड़ता है, जिसे राष्ट्रीय साहित्यकार कहा जा सकता है.
इस यथार्थ दृष्टि से गर्भित दृष्टा बंकिमचन्द्र ने पराधीनता की पीड़ा को जितनी गहराई से अनुभव किया, शायद अन्य साहित्यकारों ने नहीं.
उन्होंने ‘आनन्दमठ’ उपन्यास में देश-धर्म का दीप प्रज्वलित कर दिया था.
बंकिमचन्द्र ने अपने युग में जिस संवेदना के लिए देशप्रेम की भावना सम्भाली, वास्तव में काल में अति स्वाधीनता संग्राम के महामंत्र में वह एक महान प्रेरणा के रूप में अंकित हो गयी.
एक दृष्टिवन्त महामुनि पर ‘वन्देमातरम्’ के महामंगलोच्चार से प्राणों का संचरण हुआ.इतना ही नहीं, बंगाल के क्रान्तिकारी दलों की ‘अनुशीलन’ और ‘युगान्तर पार्टी’ बनी.
उन्होंने भी बंकिमचन्द्र के ‘आनन्दमठ’ और सन्यासी विद्रोह की महान भूमिका स्वीकार की.अन्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उन्होंने जिस राष्ट्र चेतना की न्यारा गाथा रचाई, समूचे देश को बाँधनेवाला सूत्र तथा अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्ति पाने के लिए प्रेरणा प्रदत्त की.एक साहित्यकार की रचनाओं की इससे बढ़कर क्या उपलब्धि हो सकती है? तभी श्रद्धेय बंकिमचन्द्र आज भी भारतीयों के हृदय में श्रद्धा और आदर से विराजते हैं.19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंकिम ने राष्ट्रीय भावनाओं के जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
पराधीनता के कालखंड में तन्वशील और निर्भीक ही नहीं, संघर्षशील मानस बंकिमचन्द्र के देश-भक्ति से ओत-प्रोत ओजस्वी गीत ‘वन्दे मातरम्’ ने एक बार पुनः जीवन्त हो उठा.
श्री अरविन्द ने अपने क्रांतिकारी जीवन के आरम्भ में ‘वन्दे मातरम्’ नाम से पत्र प्रकाशित किया. इस मंत्र की शक्तिधारा ने क्रांतिकारियों को जितना प्रभावित किया, उतना ही राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतन्त्रता संग्राम को.क्योंकि बंकिमचन्द्र बंगाल-साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार और उपन्यासकार थे.उनके ‘आनन्दमठ’ का ‘वन्दे मातरम्’ गीत सभी देशवासियों का कृद्घार बना हुआ है.कर्म, ज्ञान और चिंतन की जगे के लिए बंकिम ने 1879 ईस्वी में ‘बंगदर्शन’ पत्रिका का प्रकाशन किया.यह पत्र अत्यंत गंभीर और प्रगतिशील साहित्य के लिए समाज को एक नवीन उपस्थिति प्रदान करता था.अखण्ड और स्वतन्त्र भारत की पीड़ा सदा हृदय में बसती थी.इसके लेखक देवघर के प्रसिद्ध पर्यावरणविद,पक्षी विशेषज्ञ, लेखक, चित्रकार,डाक टिकट संग्रहक रजत मुखर्जी है.
रिपोर्ट रितुराज सिन्हा











.jpg)



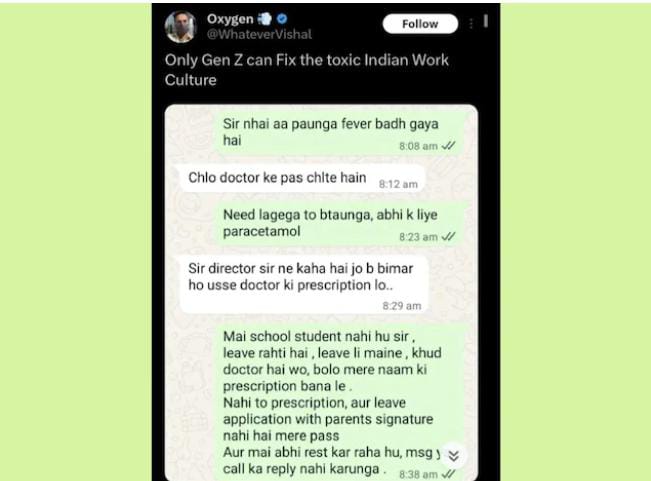
.jpeg)





Recent Comments