डॉ. जंग बहादुर पाण्डेय ’तारेश’, रांची:
यदि कविता लोक चित्त से जुडने का माध्यम है, तो नागार्जुन सही मायने में स्वाधीन भारत के जनकवि हैं. इस देश कीकरोडों-करोड़, भूखी-अधनंगी जनता की शायद ही कोई ऐसी आकांक्षा और अनुभूति हो, जिसकी ओर नागार्जुन का ध्यान न गया हो और जिस पर उन्होंने कभी गहन संवेदनात्मक और कभी तीव्र आक्रामक टिप्पणी न की हो. उन्होंने सचमुच हिंदी कविता की विषय वस्तु को अभूतपूर्व विस्तार दिया है और सुन्दर -असुन्दर सभी प्रकार के विषयों पर अपनी बेबाक टिप्पणी की है. डॉ. परमानंद श्रीवास्तव का यह कथन सोलह आने सही है:
"जनता के पक्ष में कविताएं लिखने वाले और भी हैं,पर जनता को अपने में आत्मसात् कर कविता लिखने वाले नागार्जुन अपने ढंग के अकेले कवि हैं."
नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में एक रूढिवादी मैथिल परिवार में 30 जून 1911 ई. को हुआ था. एक-एक कर चार भाइयों के बचपन में ही काल कवलित हो जाने के बाद पिता पं. गोकुल मिश्र ने वैद्यनाथ महादेव से संतान की याचना की थी. इसीलिए आगंतुक का नाम पड़ा वैद्यनाथ मिश्र. वैद्यनाथ की पढाई का श्रीगणेश तत्कालीन प्रथा के अनुसार लघु सिद्धांत -कौमुदी और अमर कोष से हुआ. फिर उन्होंने वाराणसी में रहकर संस्कृत का विधिवत अध्ययन किया. 1931 में उनका विवाह अपराजिता देवी से हो गया; लेकिन इसके केवल तीन वर्ष बाद किसी बात पर रूठकर वे घर से निकल गए. वे सिंहल जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और नाम पडा नागार्जुन.
नागार्जुन बहुआयामी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं. उन्होंने एकाधिक भाषाओं में गद्य और पद्य की अनेक विधाओं में इंद्र धनुषी साहित्य सृष्टि की है.
उनका रचना संसार
1. संस्कृत (काव्य)-कर्यालोक- शतकम्,देश -दशकम्,कृषक- दशकम्,श्रमिक- दशकम्, लेनिन- दशकम्.
2. हिन्दी-(काव्य)-युग धारा,सतरंगे पंखोवाली,प्यासी पथराई आंखें,तालाब की मछलियां, तुमने कहा था,चंदना (लम्बी कविताएं),भस्मांकुर,भूमिजा,(खंड काव्य)खिचडी विप्लव देखा हमने,पुरानी जूतियों का कोरस,हजार हजार बांहों वाली.
उपन्यास: रतिनाथ की चाची,बलचनमा,नई पौध,बाबा बटेसर नाथ,वरुण के बेटे,दुख मोचन,कुंभीपाक,हीरक -जयंती, उग्रतारा, इमरतिया, जमनिया के बाबा.
3. मैथिली ( क)काव्य: चित्रा, पत्र हीन नग्न गांछ.
(ख)उपन्यास:पारो,बलचनमा,नवतुरिया
यह ठीक है कि नागार्जुन को साहित्य में प्रारंभिक प्रतिष्ठा अपने कथा साहित्य विशेष रुप से बलचनमा(1952) नामक उपन्यास के कारण मिली; जिसमें उत्तर बिहार के एक विपन्न युवक के जीवन संघर्षों का बडा ही सजीव और बेबाक अकंन हुआ है,पर उनका कवि रूप उनके कथाकार रूप से किसी तरह घटकर नहीं है. जैसा कि डा नामवर सिंह ने लिखा है कि "नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जन कवि हैं." उन्होंने सामान्य जन के जीवन को केवल निकट से देखा ही नहीं है उसमें साझेदारी भी की है. उन्हें जनता की हर पीडा, हर बेबसी की प्रत्यक्ष अनुभूति है और उसपर अपनी गहरी प्रतिक्रिया वे निर्भीक होकर व्यक्त करते हैं;बल्कि वे केवल प्रतिक्रियाएं ही व्यक्त नहीं करते,आगे बढकर जन संघर्ष में अगुआई भी करते हैं.
कविता को माना स्थायी भाव
नागार्जुन प्रतिहिंसा को अपनी कविता का स्थायी भाव मानते हैं. समाज की हर विषमता, हर असंगति की ओर उनकी दृष्टि जाती है और वे उस पर करारी चोट करते हैं. कविता का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात हमने बहुत बार सुनी है,लेकिन उसका सबसे सचेष्ट और सबसे प्रभावी प्रयोग हिंदी में नागार्जुन ने ही किया है. मुट्ठी भर हड्डियों के ढांचेवाले इस कवि का जीवट और अंतर का ओज देखने योग्य है:
जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं?
जन कवि हूँ, मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं?
और
जनकवि हूँ मैं,क्यों चांटू मैं थूक तुम्हारी?
श्रमिकों पर मैं क्यों चलने दूं बंदूक तुम्हारी?
किसानों और मजदूरों पर चलनेवाली इस बंदूक का नागार्जुन ने अपनी अनेक कविताओं में भांति भांति से विरोध किया है. शासन की बंदूक वाली कविता में कवि ने बंदूक को दमन नीति का प्रतीक मानकर उसके अनेक चित्र खडे किए हैं:
"खडी हो गई चांप कर,ककांलों की हूक.
नभ में विपुल विराट सी, शासन की बंदूक.
और
जली ठूंठ पर बैठकर, गई कोकिला कूक
बाल न बांका कर सकी,शासन की बंदूक।।
कोकिला भी काली है और बंदूक भी. किंतु दोनों के प्रतीकत्व में कितना अंतर है।एक में जीवन का उल्लास है तो दूसरी में मृत्यु का आतंक. दोनों को समानांतर प्रस्तुत कर कवि ने मौत के शिकंजे को चुनौती देती हुई अभिनव जीवन चेतना का अत्यंत सांकेतिक और व्यजंक चित्र उपस्थित कर दिया है. जो लोग नागार्जुन की कविता कोअखबारी कतरन और नारेबाजी से अधिक महत्व नहीं देना चाहते,उन्हें ऊपर की पंक्तियां तनिक ध्यान से और पूर्वाग्रह मुक्त होकर देखनी चाहिए.

फक्कड़पन और घुमक्कड़ी प्रवृति
फक्कड़पन और घुमक्कड़ी प्रवृति नागार्जुन के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता रही है. व्यंग्य नागार्जुन के साहित्य में स्वभावतः समाहित है।चाहे सरकार हो,चाहे समाज हो या चाहे मित्र, उनके व्यंग्य वाण सबको बेध डालते हैं. कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण करने वाले इस कवि को अपनी स्पष्टवादिता और राजनीतिक कार्य कलापों के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा है.
कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नाम के दुरूपयोग पर नागार्जुन ने प्रश्न उठाया है:-
गांधी जी का नाम बेचकर,
बतलाओ कब तक खाओगे?
यम को भी दुर्गंध लगेगी,
नरक भला कैसे जाओगे?
नागार्जुन-झंडा कविता
अंदर संकट, बाहर स़कट,संकठ चारो ओर।
जीभ कटी है भारत माता,मचा न पाती शोर।
देखो धंसी धंसी ये आंखें, पिचके पिचके गाल।
कौन कहेगा आजादी के बीते तेरह साल!
नागार्जुन तो कभी सीधे सीधे आक्रोशी मुद्रा में प्रहार करते हैं, तो कभी तेवर बदलकर व्यंग्य पर उतर आते हैं. उनकी व्यंग्यात्मक कविताओं की संख्या अनगिनत है. मात्रा और बेधकता दोनों दृष्टियों से कबीर के बाद वे हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकार हैं. प्रेतका बयान, बाकी बच गया अंडा, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी,इंदुजी इंदुजी क्या हुआ आपको?, तुम रह जाते दस साल और,नया तरीका, भूले स्वाद बेर के,जयति नखरंजनी, तीनों बंदर बापू के,यंत्र कविता, आए दिन बहार के,आदि उनकी एक से एक उत्कृष्ट व्यंग्य रचनाएं हैं।आए दिन बहार के में कलयुगी नेताजी की अच्छी खबर ली गई है :-
श्वेत श्याम रतनार आंखियां निहार के,
सिंडीकेटी प्रभुओं की पगधूर झार के
लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के,
खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के।
नागार्जुन की इस तरह की कविताओं के महत्व को स्वीकारते हुए डा राम विलास शर्मा ने लिखा है कि :-“नागार्जुन ने लोकप्रियता और कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य को जितनी सफलता से हल किया है, उतनी सफला से बहुत कम कवि -हिंदी से भिन्न भाषाओं में भी -हल कर पाए हैं (अस्तित्ववाद और हिंदी कविता).“
सचमुच अखबारी समाचारों को कविता में रूपायित करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि यह बोध को अनुभव में ढालने की समस्या है. नागार्जुन की बहुतेरी कविताएं सपाटबयानी के दोष से पीडित हैं. मगर,जहाँ उनका मन सध गया है,वहाँ रचना अविस्मरणीय बन पड़ी है. जैसे अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता।इसमें कवि ने अकाल की त्रासदी और अन्न प्राप्ति के उत्सव को कम से कम शब्दों में केवल चित्रों और बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है:-
कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास,
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास;
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकिलियों की गश्त,
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त,
×××××××××××××××××××××
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद,
धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनो के बाद,
चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद,
कौए ने खुजलाई पांखे,कई दिनों के बाद।
यहां कवि ने कई खंडचित्रों को पिरोकर एक संपूर्ण चित्र तो बनाया ही है, एक ही पद की आवृत्ति से प्रभाव को घनीभूत करने में भी सफलता पायी है. मानुषी स्थिति के साथ घरेलू पशु-पक्षियों और कीट-पंतगों तक को जोड़कर अकाल की व्यापकता का भी संकेत किया है.
नागार्जुन स्वभाव से घुमंतू रहे हैं. उन्होंने देश विदेश के अनेक प्राकृतिक दृश्यों को खुली आंखों देखा है और उन्हें मार्मिकता से कलमबंद किया है. ऐसी कविताओं में 'बादल को घिरते देखा है' एक महत्वपूर्ण कविता है:-
तुंग हिमालय के कंधों पर,
छोटी बड़ी कई झीलें हैं,
उनके श्यामल नील सलिल में,
समतल देशों से आ आकर
पावस की ऊमस से आकुल,
तिक्त-मधुर विसतंतु खोजते,
हंसो को तिरते देखा है!
बादल को घिरते देखा है?
नागार्जुन जीवनपर्यंत यायावर जरूर रहे, लेकिन उनकी कविता में गार्हस्थिक जीवन का आकर्षण कम नहीं है. सिंदूर तिलकित भाल, यह दंतुरित मुस्कान, तन गई रीढ़, गुलाबी चूड़ियाँ आदि कविताएं पारिवारिक भावोष्णता से परिपूर्ण हैं. संक्षेप में नागार्जुन की कविता की संवेदना का वृत अत्यंत व्यापक है. उसमें महाकवि कालिदास से लेकर मादा सूअर तक का अंटाव है. एक ओर यदि नागार्जुन कालिदास से प्रश्न पूछते हैं:-
कालिदास सच सच बतलाना,
इंदुमती के मृत्यु शोक से
अज रोया या तुम रोए थे?
तो दूसरी ओर मादा सूअर से भी सहानुभूति रखते हैं:-
जमुना किनारे मखमली दूबों पर,
पूस की गुनगुनी धूप में,
पसर कर लेटी है
यह भी तो मादरे हिंद की बेटी है,
भूरे-पूरे बारह थनोवाली।
नागार्जुन जनकवि होने के साथ अत्यधिक अधीत और सुपठित कवि हैं. लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं, विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है. छायावादोत्तर काल के वे अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती हैं. जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज संप्रेषणीय और प्रभाव शाली होती हैं कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती हैं।नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है।जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है.
नागार्जुन ने छंद बद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं. उनकी काव्य भाषा में एक ओर संस्कृत काव्य परम्परा की प्रतिध्वनि है, तो दूसरी ओर बोल चाल की भाषा की रवानी और जीवंतता भी।उनके कंधे पर लटक रहे खादी के झोले में एक तरफ कालिदास का मेघदूतम मिलेगा तो दूसरी तरफ मार्क्स, लेनिन और टाल्सटाय की रचनाएं भी.
नागार्जुन अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजे गए हैं. पत्रहीन नग्न गांछ (मैथिली कविता संग्रह) के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत- भारती पुरस्कार, मध्यप्रदेश सरकार ने मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार ने राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया.
भारतीय काव्य परम्परा का जीवंत रूप
नागार्जुन के काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परम्परा जीवंत रूप में उपस्थित देखी जा सकती है. उनका कवि व्यक्तित्व कालिदास और विद्यापति जैसे कालजयी कवियों के रचना संसार के गहन अवगाहन, बौद्ध एवम् मार्क्सवाद जैसे बहुजनोन्मुख दर्शन के व्यावहारिक अनुगमन तथा सबसे बढ़कर अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं और संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ाव तथा लोक संस्कृति एवम् लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है।उनका यात्रीपन भारतीय मानस एवम् विषयवस्तु को समग्र और सच्चे रूप में समझने का साधन रहा है. मैथिली, हिंदी और संस्कृत के अलावा पालि, प्राकृत, बंगला सिंहली,तिब्बती आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान भी उनके इसी उद्देश्य में सहायक रहा है. उनका गतिशील सक्रिय और प्रतिबद्ध सुदीर्घ जीवन उनके काव्य मे जीवंत रूप में प्रतिध्वनित एवम् प्रतिबिंबित है. नागार्जुन सही अर्थों में सर्वतोभावेन आधुनिक जनकवि हैं, वे न किसी से डरने वाले कवि हैं न जनपथ से डिगने वाले. उनकी यह स्पष्ट घोषणा इसी बात का द्योतक है:-
जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ?
जनकवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं!
संदर्भ-ग्रंथ:-
1. नागार्जुन-रचनावली, राजकमल प्रकाशन,नई दिल्ली 1975
2. नागार्जुन का रचना संसार सं. विजय बहादुर सिंह, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2009
3. नागार्जुन की कविता, डॉ. अजय तिवारी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2005
4. नागार्जुन का कवि-कर्म, डॉ. खगेन्द्र ठाकुर,प्रकाशन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली,2001
5. नागार्जुन:अंतरंग और सृजन-कर्म, सं. डॉ. मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद 2005
6. आलोचना(सहस्त्राब्दी अंक,43,अक्टूबर-दिसबंर 2011)सं. डॉ. अरुण कमल,राजकमल,प्रकाशन, नई,दिल्ली
7. तुम चिर सारथि यात्री(नागार्जुन-आख्यान) ताराचंद नियोगी, अंतिका प्रकाशन, दिल्ली 2010
8. युगों का यात्री(नागार्जुन की जीवनी) ताराचंद नियोगी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली,2008
9. सुकवि- समीक्षा, डॉ. आनंद नारायण शर्मा, भारती भवन,पटना,1978

(लेखक पूर्व अध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में HOD रहे हैं.)





.jpeg)

.jpeg)










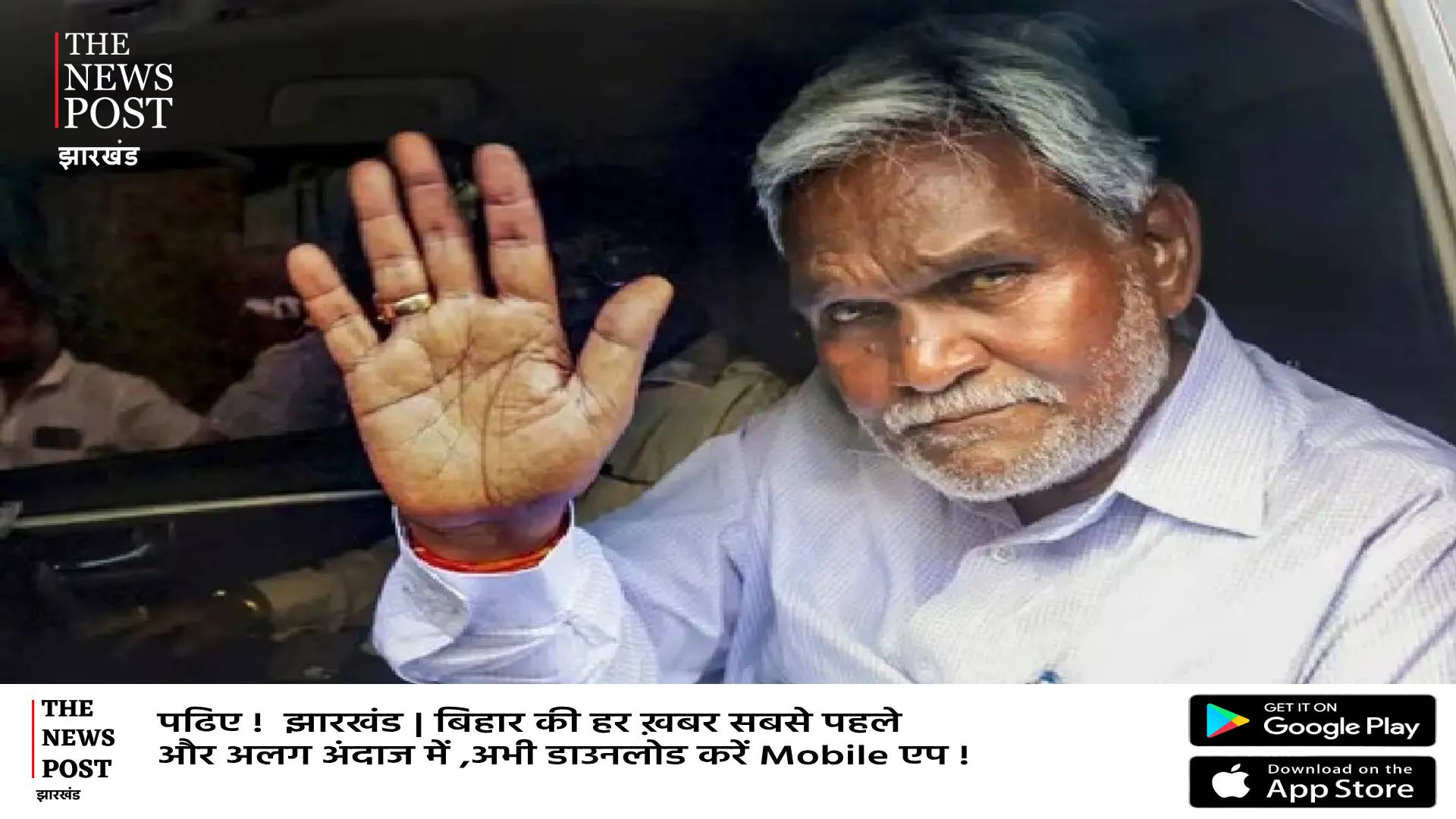


Recent Comments